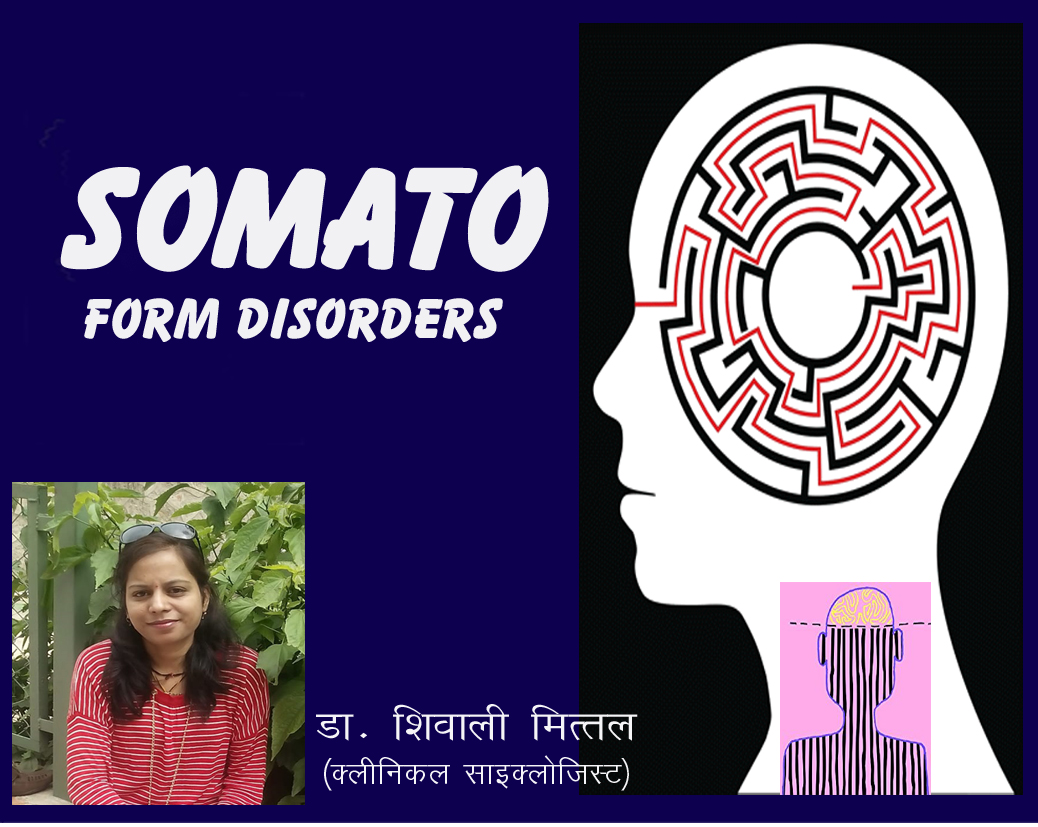लेखक : ज्ञानेन्द्र रावत
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।
www.daylife.page
दुनियाभर के ग्लेशियर खत्म होने के कगार पर हैं। वे तेजी से पिघल रहे हैं बल्कि खोखले भी हो रहे हैं। अगर इनके पिघलने और खोखले होने की यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में दुनिया एक एक बूंद पानी को तरस जायेगी। दरअसल जलवायु की प्रचंड आंधी ग्लेशियरों को निगल रही है। यह महज बर्फ का पिघलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुनामी है जो हमारी दुनिया को उलट-पुलट करने को तुली है। इससे जहां बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ जाता है, वहीं इससे बुनियादी ढांचे के साथ साथ कृषि उत्पादन,जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। वैज्ञानिकों की मानें तो 2000 से लेकर 2023 के बीच बर्फ के यह पहाड़ जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, 650,000 करोड टन बर्फ खो चुके हैं। यह सिलसिला थमा नहीं है, लगातार जारी है। वेनेजुएला पहला देश है जिस पर जलवायु परिवर्तन का इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिये। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमरीका में 20 वीं सदी के मध्य में कम से कम 400 ग्लेशियर गायब हो गये। ग्लेशियर पिघलने के मामले मे वह चाहे अंटार्कटिका हो, आर्कटिक हो, ग्रीनलैंड हो, आल्पस हो या राकीज,आइसलैंड हो, हिंदूकुश हो या फिर स्विट्जरलैंड हो या ब्रिटेन हो, हरेक की हालत एक जैसी ही है। कहीं कोई बदलाव नहीं है।
साल 2010 के पहले आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो बर्फ की चादर बिछी होती थी, उसमें अब लाखों वर्ग किलोमीटर की कमी हो गयी है। अब आर्कटिक में केवल 143 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ बची है। अंटार्कटिका का सबसे बडा हिमखंड ए 23अपनी जगह से फिर खिसक रहा है। इसका आकार 3672 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमखंड महासागरों की धाराओं द्वारा बहाकर लाया गया है और यह अभी दक्षिण जार्जिया के गर्म जल की ओर बढ़ रहा है और यहां यह टूटकर पिघलने की प्रक्रिया में है। यह यहां उत्तरी महासागर में महीनों फंसे रहने के बाद फिर से अपनी जगह से खिसक रहा है। बर्फ के प्राकृतिक रूप से बढ़ने की क्रिया के कारण यह हिमखंड टूटकर अलग हुआ है हांलाकि इससे समुद्र के जलस्तर में कोई बदलाव नहीं आयेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है जिसने समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है।
ग्रीनलैंड की हालत तो और हैरान कर देने वाली है। वहां बीते 13 साल में 2,347 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ गायब हो गयी है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया को भरने के लिए पर्याप्त है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से दुनियाभर में समुद्र के जलस्तर में बदलाव हुआ, साथ में मौसम के पैटर्न में भी बदलाव सामने आया है। इसका असर दुनियाभर के ईकोसिस्टम और समुदायों पर हुआ है। स्विटजरलैंड के प्रसिद्ध रोन ग्लेशियर सहित आल्पस पर्वत श्रृंखला के कई ग्लेशियरों में बर्फ के नीचे अजीबोगरीब सुरंगें और गड्ढे हो गये हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति दुनियाभर के ग्लेशियरो की हो सकती है। तेजी से बढ़ रहे तापमान के कारण अब ग्लेशियर सिर्फ पिघल नहीं रहे हैं, वे अब भीतर से खोखले भी हो रहे हैं। ग्लेशियर मानीटरिंग समूह ग्लैमास के प्रमुख एवं ज्यूरिख के ई टी एच जैड इंस्टीटयूट के व्याख्याता मैथिलस हुस ने कहा है कि पहले छेद बर्फ के बीच बनते हैं और फिर वे बड़े बनते हैं। हिंदूकुश क्षेत्र के ग्लेशियर से नवम्बर से मार्च तक बर्फ में 23.6 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुयी है। यह बीते 23 सालों में सबसे कम है। नतीजतन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। बर्फबारी में यह गिरावट लगातार तीसरे साल दर्ज की गयी है।
जलवायु बदलाव और स्थलाकृति के कारण मध्य हिमालय का एक ग्लेशियर तेजी से खिसक रहा है। लम्बे समय से पिघल रहे ग्लेशियरों की चिंताओ के बीच यह नया संकट है। दरअसल ग्लेशियर आगे की ओर खिसकने की घटनाएं अभी तक अलास्का, कराकोरम और नेपाल से सामने आती थीं। वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग, तापीय इफेक्ट और उस इलाके की टोपोग्राफी को मुख्य वजह मान रहे हैं। वैज्ञानिक इस ग्लेशियर का उद्गम भारत में और निकास तिब्बत की ओर मानते हैं। इससे तिब्बत से लेकर धौलीगंगा तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिक ग्लेशियर में इस बदलाव की स्थिति को निचले इलाकों के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं। ऐसी घटनायें आबादी क्षेत्र में भीषण बाढ़ और तबाही का सबब बन सकती हैं। देखा जाये तो सर्दी के दौरान आमतौर पर जहां बर्फ दिखाई देती थी, वह या तो बहुत तेजी से पिघल रही है या अपेक्षित मात्रा में पड़ ही नहीं रही है।
असलियत में ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर मौजूद ग्लेशियरों पर तो नुक़सान पहुंचा रही है, वह हिमालयी क्षेत्र में 37,465 वर्ग किलोमीटर में फैले कुल 9575 ग्लेशियरों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है जो अब तेजी से पिघलने लगे हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्र मे जमे ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे एशिया की जल मीनार और विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते है। यह दक्षिण एशिया में 160 करोड लोगों की जलापूर्ति का आधार है। एशिया की 10 प्रमुख नदियों को पानी देने वाले इन ग्लेशियरो से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी तीन नदियां विभाजित हुयी हैं। कश्मीर में भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यहां भी पानी का संकट है। यहां लिद्दर नदी का मुख्य स्रोत कोलाहोई ग्लेशियर और तेजवान ग्लेशियर का दायरा ढाई किलोमीटर से भी ज्यादा घट गया है। इससे सबसे बड़ा खतरा यह हुआ है कि पहाडों पर कई छोटी-छोटी झीलें बन गयी हैं जो ज्यादा हिमस्खलन की स्थिति में कभी भी फट सकती हैं। इसरो की रिपोर्ट को मानें तो हिमालय की 2432 ग्लेशियर झीलों में से 676 का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इनमे से भारत में मौजूद 130 झीलों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रह है जो खतरनाक संकेत है। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलें खतरे की घंटी बजा ही रही हैं। फिर नदियों का जलस्तर भी कम हो रहा है। यह चिंतनीय है। गौरतलब कि सूखे के मौसम में यही बर्फ नदियों में पानी का स्रोत होती हैं। ऐसे में बर्फ में इस भारी गिरावट का असर भारत या आसपास के देशो के लगभग दो अरब लोगों की जलापूर्ति पर पड़ेगा। यह कहना है अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का। उसका मानना है कि कार्बन उत्सर्जन इस इलाके में बर्फ की कमी का कारण है। इसके लिए तत्काल विज्ञान आधारित व दूरदर्शी नीतियों संग एक आदर्श बदलाव लाने की जरूरत है।
साथ ही सीमापार जल प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए नये सिरे से क्षेत्रीय सहयोग को बढावा देने की भी जरूरत है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि आमतौर पर नदियों के पानी का 23 फीसद हिस्सा बर्फ पिघलने से आता है लेकिन इस बार बर्फ में सामान्य से 23.6 फीसदी की गिरावट चिंतनीय है जबकि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी 12 नदी बेसिनो में यही स्थिति है। यूनेस्को ने भी चेताया है कि ग्लेशियरो के पिघलने की यदि मौजूदा दर बनी रही तो इसके परिणाम अभूतपूर्व और विनाशकारी होंगे। ग्लेशियरों की इस बदहाली को देखते हुए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि वे ग्लेशियर बचाने हेतु आगे आयें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्लेशियर बचाने हेतु जल्द कदम उठाना जरूरी है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि हमारी बारहमासी नदियों का स्रोत यही ग्लेशियर हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद हिमालय में पृथ्वी पर यह बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो 144 सालों बाद अगला महाकुंभ संभवत रेत पर आयोजित करना होगा। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)