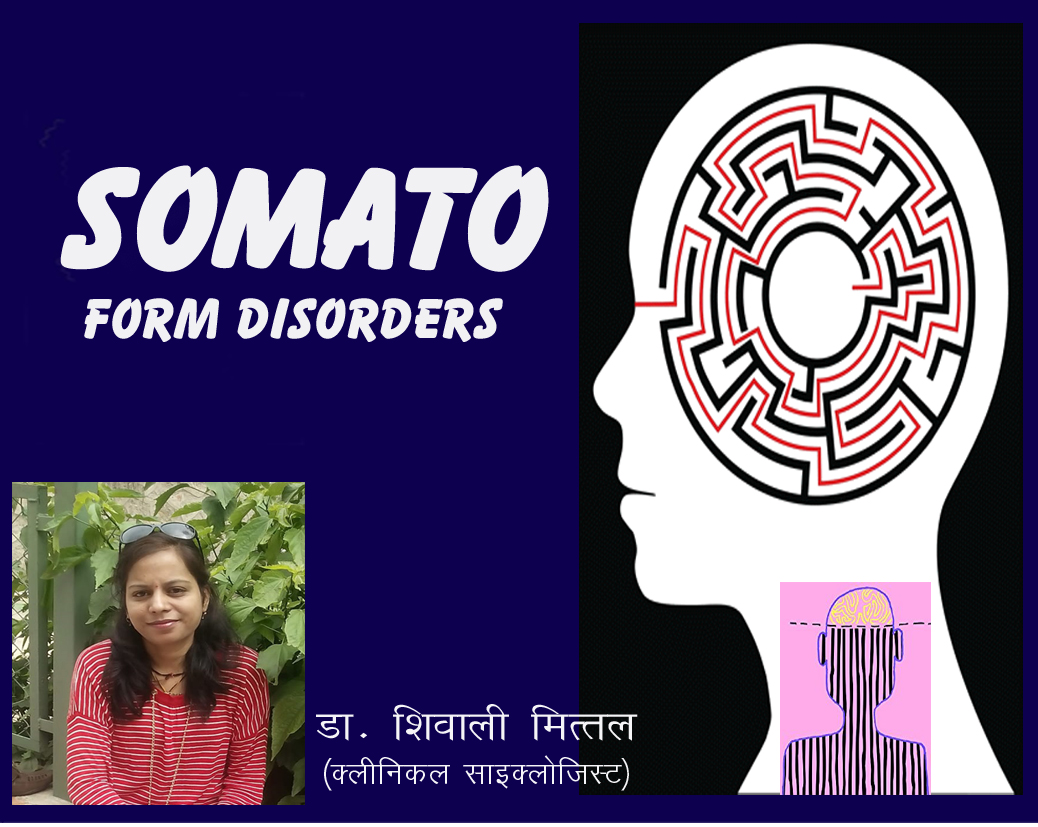लेखक : वेदव्यास
लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं
www.daylife.page
जब से खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने हमारे देश में प्रवेश किया है तब से सब कुछ ‘भगवान भरोसे‘ हो गया है। सामाजिक सरोकार का स्थान निजी सरोकार ने ले लिया है। विकास अब भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो गया है तथा सरकार और संविधान की जगह अब निजी व्यापार और प्रतियोगिता के बाजार ने ले ली है। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे अब जहां मनुष्य के मन, वचन और कर्म पर पड़ रहा है वहां इसने हमारे साहित्य, सरोकार और संवेदनाओं के धरातल को भी अव्यवस्थित कर दिया है।
साहित्य लेखक इस परिस्थिति के चक्रव्यूह में फंसे उस अभिमन्यु की तरह है जो निरंतर इस बात से चिंतित है कि अब वह शब्द और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए और फिर पूंजी बाजार और उपभोक्तावाद की खिड़की पर अपनी रचनाएं लेकर खड़ा हो जाए। यह बात भी बेहद सत्य है कि सत्ता और व्यवस्था विरोध की उसकी भूमिका, देश के राजनैतिक दलों से भी पुरानी है तथा उसने मनुष्य की रक्षा में सदैव-सदैव एक संत और सूरमा की तरह विचार की तलवार चलाई है। यही कारण है कि वह तात्कालिकता से विचलित नहीं रहकर सदैव उस मानवीय शाश्वत की तलाश में ही सक्रिय रहा है जिसे हम वैदिक काल से जारी लोक मंगल का ही सतत रूपांतरण मानते हैं। मध्यकाल की निर्गुण भक्ति धारा और बीसवीं शताब्दी की प्रगतिशील चिंतन असमानताओं की अशांति है तब तक एक लेखक का ‘विपक्ष‘ में बैठना ही उसकी नियति है तथा शब्द और सृजन का अनहदनाद ही उसका फलितार्थ है।
हमने इससे पहले ऐसे दृश्य विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में, कभी नहीं देखे कि लेखक और साहित्य की भूमिका पर सरकार और बाजार हावी हो जाएं। लेकिन आजादी के बाद इन 75 वर्षों में प्रायः यह देखने में आया है कि साहित्य में व्यक्तिवाद, प्रचारवाद, पुरस्कारवाद, सत्तावाद और संस्थावाद की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ी है तथा राजा-बादशाहों के समय में स्थापित लाखपसाव और गांव जागीर की मनसबदारी भी अब कुछ लेखकों के हाथ से निकलकर अधिकांश लेखकों की चिंता और आवश्यकता का विचार बिंदु बन गई है। रचनाकार की रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगी है तथा कमबेशी मूल्य और मान्यताओं की जगह उसने अवसर और सुविधा के जीवन अनुवाद को स्वीकार कर लिया है।
आज लेखक और सृजनकर्ता जंगल में जोगी की तरह नहीं रहता और धीरे-धीरे उसका झुकाव शोषण करने वाली राज्य शक्तियों के खिलाफ तटस्थता और तालमेल के लिए बढ़ता जा रहा है। वह अब पाब्लो नरूदा, मैक्सिम गोर्की, ताल्सताय, सोलजिनसिन, सुब्रहण्यम भारती अथवा प्रेमचंद की तरह नहीं बनना चाहता है। उसकी कृतियों का ताना बना अब बारीक मानवीय मनोविज्ञान पर केंद्रित नहीं रहता तथा एक जल्दी में वर्तमान और तत्काल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है।
हमारे देश में साहित्य और भाषा की यह आपसी कलह इस बात से भी समझी जा सकती है कि यहां तरफ 60 प्रतिशत निरक्षरों के महान समाज में आज भी अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का साहित्य और लेखक ही अधिक बिकता और सम्मानित होता है तो वहां दूसरी तरफ गीता प्रेस, गोरखपुर जैसे धर्म-अध्यात्म के संस्थान ही आज भी गांव-गांव और घर-घर तक भाग्य, भगवान और भय को स्थापित करने वाले और नौकरी-चाकरी से थक जाने के बाद कविता-कहानी और नाटक-उपन्यास लिखने वाला लेखक, रंगकर्मी और ललित कलाओं का सूत्रधार धीरे-धीरे आत्मप्रवंचना, आत्मविडम्बना और अंतर्विरोधों का शिकार होता जा रहा है। आधुनिक काल और उत्तर आधुनिक काल पर बहस करते-करते उसके हाथ से सामाजिक और मानवीय भविष्य की सारी पहल निकलती जा रही है तथा लेखक का अवचेतन भी अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त होता जा रहा है।
आप कभी सोचिए कि आज लेखक की इस मनोदशा का क्या कारण है कि वह पढ़ता कम है और लिखता ज्यादा है। वह जनता से मिलता कम है और जनता की वकालत अधिक करता है और वह परम्परा और संस्कृति के रचनात्मक द्वंद्ध को समझे बिना ही वर्तमान के दबाव से अधिक चिंतित रहता है। वह अपने सृजन पर केंद्रित रहने की जगह प्रचार और प्रकाशन माध्यमों के गलियारों में अधिक समय बिताता है। वह जैसा कहता है वैसा लिखता नहीं है और जैसा लिखता है, वैसा दिखता नहीं है। यानी कि समाज और मनुष्य के समयगत अंतर्विरोधों से लड़ने वाला सैनिक-लेखक अब खुद सबसे अधिक अस्त-व्यस्त और ध्वस्त क्यों है? वह धैर्य से गुमनामी के समुद्र में सत्य के मोती क्यों नहीं ढूंढ़ना चाहता है और उसकी ऐसी क्या विवशता है जो कि वह सुख की आधी रोटी को छोड़कर दुःख की पूरी रोटी के पीछे दौड़ रहा है।
हमें अब इस भटकाव पर भी विचार करना चाहिए कि एक लेखक द्वारा अपने ही चंदे और विज्ञापन की राशि से जीते जी स्वर्ण जयंती मनवाने की क्या सार्थकता है। एक लेखक द्वारा अपनी पुस्तक का लोकार्पण एक सत्ता पुरुष और वाणिज्यदूत के करकमलों से करवाने की क्या विवशता है। एक लेखक के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी अथवा किसी अखबार के दफ्तर में बैठे तथाकथित संपादक की चापलूसी करने का क्या औचित्य है। एक लेखक को यह भी तो सोचना चाहिए कि जब पुस्तक के पाठक ही नेस्तानाबूद हो रहे हैं तब वह अज्ञानी प्रकाशकों के घर पर चक्कर क्यों लगा रहा है। उसे यह भी तो जानना चाहिए कि लाख-पचास हजार अथवा पांच और ग्यारह हजार रुपए का पुरस्कार देने वाला व्यक्ति और संस्थान आखिर उसकी रचना/कृति को श्रेष्ठ कैसे साबित कर देगा। फिर इसके अलावा एक लेखक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि लेखक की शक्ति उसके शब्द जीवन में है। चिंतन की अंर्तसाधना में है तथा मनुष्य के भीतर बनते-बिगड़ते सुख-दुःख में ही निहित है।
शेक्सपीयर, कालिदास, तुलसीदास अथवा कबीर तो कभी किसी सिंहासन के गायक और वादक नहीं रहे लेकिन आज भी उन्हें क्यों पढ़ा समझा जाता है। पुस्तक की भूमिका लिखने वाला आचार्य प्राचार्य से कहीं बड़ा जब उस कृति का लेखक ही होता है तब एक रचनाकार अपने घट में कस्तूरी मृग की तरह है। और ऐसी ही बहुत ही विचलन और फिसलन आज हमारे रचनाकर्म पर हावी है-जिसे देखकर लगता है कि साहित्य की अवधारणा सिमट रही है तथा इस लोक से परलोक तक के सभी रास्ते एक लेखक को ईमानदार बने रहने में बाधा डाल रहे हैं। लेखक का सम्पूर्ण मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भला इस मायावी और तत्काल के यशस्वी प्रपंच में कैसे बचे यह हमारी आज की चिंता का मूल कारण है। आखिरकार एक रचना का भूत, भविष्य और वर्तमान तो उसके शब्द संसार में ही जनमता और मरता है अतः एक लेखक का मन और विचार तो उस पानी की तरह है जो सदैव ढलान की ओर बहता है और सत्य और सौंदर्य की सम्पूर्णता की ओर ही चलता है।
मैं इस बात से कतई-सहमत नहीं हूं कि ज्ञान विज्ञान और वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास से शब्द लेखक का और हमारे सरोकारों का बुनियादी संसार बदल जाता है। कुछ लोग आजकल साहित्य में भी ‘प्रोफेशनलिज्म‘ (पेशेवरता) की दुहाई देते हैं लेकिन प्रकृति और मनुष्य का मूल-सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि साहित्य सृजन कोई पेशा और धंधा नहीं है तथा यह एक ऐसे मानव समाज की खोज है जिसमें पाने और खोने के सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं तथा लेखक एक नीर, क्षीर, विवेक के स्तर पर अपने लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मनुष्य जीवन की खुशहाली के लिए अनवरत शब्द कर्म और विचार कर्म की साधना करता रहता है। वह एक शाश्वत और दर्शन के विराट में जीता है।
साहित्य का इतिहास तो हमें यही बताता है कि यदि आपकी वैचारिक जड़ें मजबूत होंगी तो फिर आपको उपेक्षा और असत्य की कोई भी आंधी नहीं उखाड़ सकेगी। फिर साहित्य और सृजन में खोया पाया जैसी भी कोई अवस्था नहीं होती तथा शाश्वत की इस अमर खोज में एक लेखक को निरंतर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह जिन जीवन मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को मनुष्य में देखना चाहता है, उन्हें वह सबसे पहले अपने आप में स्थापित करें। जो नहीं है उसे मनुष्य की गहरी परम्परा में खोजें तथा सभी जटिलताओं और संकीर्णताओं को लांघकर धैर्य के साथ अपने शब्द और चेतना को अंगद के पांव की तरह रोप दें।
वस्तुतः आज का लेखकीय संकट ही यह है कि रचनाकार को अपने आप पर ही भरोसा नहीं है तथा वह अखबार में और विचारों में कोई अंतर ही नहीं समझता। वह कविता, कहानी और विधाओं की संवादहीन दीवारों में कैद होने लगा है तथा वह समय से बचने के लिए व्यापक और मनुष्यगत सच्चाइयों की कुर्बानी देने लगा है। वरना क्या कारण है कि कविता की प्रासंगिकता और कहानी की वापसी जैसे प्रश्न खड़े करके हम खुद उसके उत्तर ढूंढ़ने में उलझे हैं। एक लेखक के पास सात समंदर पार झांकने की शक्ति भले ही नहीं हो लेकिन वह पहले अपने भीतर तो झांक ले। आखिर पहचान, मान्यता, स्थापना और स्मृति बनने का महाभारत वह खुद क्यों लड़ रहा है। यह सारा काम एक लेखक को अपने श्रेष्ठ सृजन पर और मनुष्य के प्रति अपने ठोस सरोकार पर छोड़ देना चाहिए। आखिर एक साहित्य सम्मेलन और महामूर्ख सम्मेलन में तो हमें फर्क रखना ही पड़ेगा।
अनुभूति और अन्तर्द्वन्द्व का यह संग्राम निश्चय ही समसामयिक परिवेश और प्रवृत्तियों के प्रदूषण से प्रभावित भी होता है लेकिन एक लेखक के लिए भी पहचान और सृजन की कुछ अनिवार्यताएं हैं। साहित्य के उद्देश्य और विचार की परम्परा पर भी सोचा जाना चाहिए। वाचिक और प्रकाशित साहित्य के अलावा भी तो चेतना के कई स्तर और रूपाकार होते हैं। भला यह दीनता और पलायन किसी लेखक का गुण नहीं हो सकते कि वह खुद ही अपना व्यक्तित्व और कृतित्व थैले में उठाकर किसी ‘नगरश्री‘ के सम्मुख नतमस्तक खड़ा हो जाय तथा वैसा ही सब कुछ गाने लगे जैसी कि हवा चल रही है।
आखिरकार एक साहित्य लेखक में, व्यापारी में, कर्मचारी में और बंदूकधारी में कोई अंतर तो होना चाहिए। रामायण और महाभारत अथवा श्रीमद्भागवत गीता जैसी अमर कृतियां आप भले ही न लिख सके लेकिन मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य होने जैसा तो कुछ लिखें और दिखें। साहित्य की प्रासंगिकता तय करने का काम किसी बाजार और प्रचारतंत्र को भला कैसे सौंपा जा सकता है। हम आंधी से पहले ही उखड़ते हुए भला एक ‘लेखक‘ कैसे बने रह सकते हैं और यथार्थ की उपेक्षा करके भ्रम के बल पर कितने समय तक जी सकते हैं। क्योंकि सृजन एक सतत मानवीय संस्कृति का संवाद है तथा इसमें लोक कल्याण की खोज के अतिरिक्त जो कुछ भी बीच में आता जाता है वह नितांत नकारात्मकता है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)