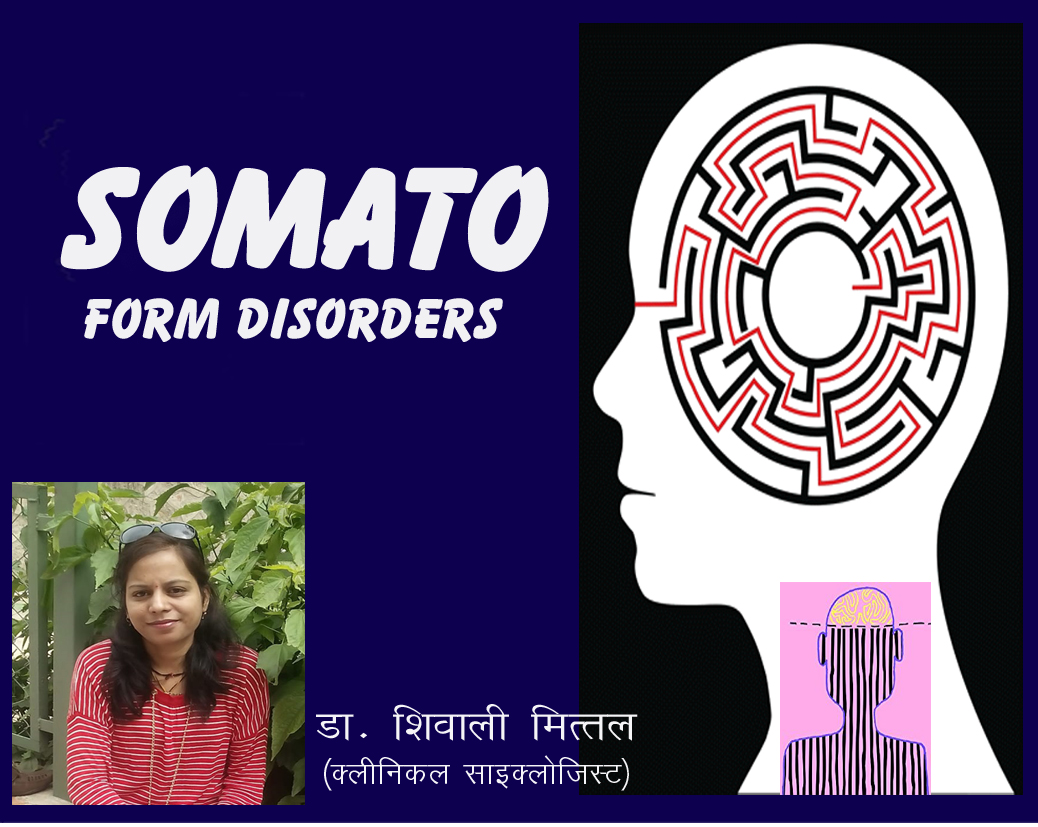लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।
www.daylife.page
देश में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात की भयावहता का सबूत यह है कि प्रदूषण के मामले में हमारा देश और देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। वह चाहे पहाड़ हो या मैदानी इलाका, तराई का इलाका हो या फिर देश का समुद्री तटीय इलाका,कोई भी प्रदूषण की मार से अछूता नहीं रहा है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि देश में हवा अब इतनी प्रदूषित है जिसकी वजह से सांस लेना भी दूभर हो गया है। देश की शीर्ष अदालत ने भी इस बाबत गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालात इतने खराब हैं कि अगर उस माहौल में आपने सांस भी ले ली तो निश्चित मानिए कि आप गंभीर प्रदूषण से श्वांस,फेफडो़ं के कमजोर होने, फेफड़े के कैंसर, हृदय, धमकियों में खून का थक्का जमने, काला दमा, ब्रेन स्ट्रोक, विटामिन डी के घटते स्तर से हृदय सम्बन्धी रोगों में हो रही बढ़ोतरी, आंखों व त्वचा के संक्रमण, समय पूर्व प्रसव और कम वजन के बच्चों के जन्म होने जैसी बीमारियों के चलते होने वाले जान के जोखिम से बच नहीं सकते। यही नहीं इससे मानसिक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी आफ सेंट एण्ड्रयूज द्वारा किये शोध से यह खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण से हवा में मौजूद दूषित कणों के दिमाग पर हमला करने से उदासी, छात्रों में पढाई संबंधी परेशानियों और जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता लगातार कम हो रही है। दुनिया के शोध- अध्ययन प्रमाण हैं कि वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य को बेहद गंभीर स्थिति तक नुकसान पहुंचाने का प्रमुख कारण बन गया है।
जहरीली हवा हर साल देश में होने वाली करीब 15 लाख लोगों की जान ले रही है। यही नहीं इसके चलते इंसान की उम्र 11.9 साल कम हो गयी है। हालात की भयावहता का प्रमाण है कि देश के केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तक ने स्वीकार किया है कि उनको देश की राजधानी दिल्ली में रहना पसंद नहीं है। इसीलिए मेरा यहां आने का मन नहीं करता। इसकी अहम वजह यह है कि यहां प्रदूषण की वजह से मुझे संक्रमण हो जाता है। यहां हर बार आते हुए लगता है कि मुझे यहां आना चाहिए कि नहीं। इतना भयंकर प्रदूषण है यहां। यह जहरीली हवा का ही नतीजा है कि अस्पतालों में सांस के रोगियों की तादाद में 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुयी है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। खासकर सांस के रोगियों में तो हर उम्र के लोग शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सुबह-शाम सैर करने वाले लोगों ने दमघोंटू हवा से बचने के लिए सैर करने जाना भी छोड़ दिया है। वायु प्रदूषण ने तो इंसान क्या ऋतुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ऋतुओं को तो वैश्विक तापमान और प्रदूषण ने हमारे वातावरण तक को बीमार बना दिया है। नतीजतन हम मौसम सम्बन्धी तमाम चुनौतियों का सामना करने को विवश हैं। मौसम में आ रहा बदलाव इसका अहम कारण है। इस सबके लिए इंसानी गतिविधियां ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं जो इंसानों पर ही भारी पड़ रही हैं। पोलैंड के रोकला यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ एण्ड स्पोर्ट्स साइंस के वैज्ञानिकों ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि इंसानी गतिविधियों के चलते न केवल महासागरों का रंग बदल रहा है बल्कि पर्यावरण में इंसानी दखलंदाजी उसी की जान की दुश्मन बन रही है। जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फार कैमिस्ट्री के शोध में यह आशंका व्यक्त की गयी है कि बढ़ते तापमान और वायु प्रदूषण पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे हर साल दुनिया में करीब तीन करोड़ लोग असमय मौत के मुंह में चले जायेंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो वार्षिक मृत्यु दर सदी के अंत तक अनियंत्रित हो सकती है और दुनिया की 20 फीसदी आबादी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करेगी।
दरअसल वायु प्रदूषण देश में हर घंटे 240 लोगों और 20 बच्चों की जान ले रहा है। यूनिसेफ़ और हैल्थ इफैक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'स्टेट आफ ग्लोबल एयर-2024' ने इसे साबित कर दिया है। प्रदूषण के कारणों के बारे में माडलिंग अर्थ सिस्टम एण्ड इनवायरमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया है खासकर उत्तर भारत के शहरों में आवासीय इलाकों और परिवहन से सबसे अधिक प्रदूषण फैल रहा है जबकि पश्चिमी भारत में उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इन क्षेत्रों में हवा में पी एम 2.5 की मात्रा बढ़ रही है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनियां में होने वाली कुल मौतों में 12 फीसदी मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। इनमें पी एम 2.5 यानी हवा में घुले महीन कणों यथा ओजोन यानी ओ3 और नाइट्रोजन डाईआक्साइड यानी एन ओ 2 जैसे प्रदूषकों की अहम भूमिका होती है। असलित्यत में ऐसे सूक्ष्म कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, फेफड़ों में रह जाते हैं और रक्त प्रवाह के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे शरीर की कई अंग प्रणालियां प्रभावित होती हैं और हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर, क्लिनिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी जैसे गैर संचारी रोगों का जोखिम बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है।
यह भी कि वायु प्रदूषण से होने वाली वैश्विक मौतों में 90 फीसदी यानी 78 लाख से ज्यादा का कारण पी एम 2.5 ही है। गौरतलब है कि यही प्रदूषण ग्रीनहाउस गैस का भी हिस्सा बनते हैं जो धरती को गर्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट को माने तो देश की 99 फीसदी से ज्यादा आबादी खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पी एम 2.5 को लेकर जो मानक बनाया है उसके अनुसार भारत की हवा 5 गुणा ज्यादा खराब है। इनमें परिवहन, घर, जंगलों की आग और उद्योगों आदि में जलाये जाने वाले जीवाश्म ईंधन और बायोमास की प्रमुख भूमिका है। असलियत यह है कि अब वायु प्रदूषण भयावह स्थिति तक जानलेवा हो गया है। यदि देश के दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई सहित 10 बड़े शहरों यानी अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, शिमला और वाराणसी का जायजा लें तो पाते हैं कि इन शहरों में हर साल तकरीब 34,000 मौतें वायु प्रदूषण के चलते होती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब देश के 10 बड़े शहरों की हालत यह है तो पूरे देश के छोटे शहरों और कस्बों-गांवों का वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा क्या होगा? लैंसेट प्लेनेटरी हैल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित शहरों में औसतन हर दिन होने वाली मौतों में से 7.2 फीसदी का संबंध हवा में मौजूद धूल के कण पी एम 2.5 से है। रिपोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत को अपने नागरिकों को प्रदूषित हवा के खतरों से बचाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप लाने के लिए काफी गंभीर प्रयास करने होंगे। भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को और कडा़ करने के लिए जुट जाना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रत्येक क्यूबिक मीटर हवा में पी एम 2.5 में हर 10 माइक्रोग्राम की बढ़ोतरी से रोजाना मृत्यु दर में 1.42 फीसदी की वृद्धि हो रही है। अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण से मरने वालों में देश की राजधानी दिल्ली सर्वोच्च स्थान पर है। यहां हर साल 12,000, मुंबई दूसरे स्थान पर जहां 5091 मौतें हो रही हैं जबकि कोलकाता तीसरे तथा चेन्नई चौथे स्थान पर है। यहां इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण का स्तर भी रोजाना मृत्यु दर का कारण बनता है। एमडीपीआई के "एयर" जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण 60 फीसदी पी एम 2.5 है।
आई क्यू एयर की रिपोर्ट इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि हमारा देश दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शुमार है और वह दुनिया में तीसरे पायदान पर है। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में सबसे सबसे प्रदूषित राजधानियों में शीर्ष पर है। हकीकत यह है कि बढ़ता प्रदूषण जहां पर्यावरणीय चुनौतियों को और भयावह बना रहा है, वहीं आबादी के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढा़ने में भी अहम भूमिका निबाह रहा है जिससे अनचाहे होने वाली मौतों में बेतहाशा बढो़तरी दर्ज हो रही है। इसके पीछे पी एम 2.5 कणों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका आकार 2.5 माइक्रोन के करीब होता है। इसके बढ़ने से धुंध छाने, साफ न दिखाई देने, सांस के रोगों, गले में खराश होने, जलन और फेफडो़ं की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जो जानलेवा साबित होती हैं। असलियत में अपने छोटे आकार के कारण पार्टीकुलेट मैटर फेफडो़ं में आसानी से गहराई तक पहुंच जाते हैं जो पी एम 10 से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। यह भी कड़वा सच है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर्यावरण में प्रदूषण का जहर तो घोल ही रहे हैं, वे मानव स्वास्थ्य के भी दुश्मन साबित हो रहे हैं। फिलहाल हकीकत यह है कि भारत लगातार वायु गुणवत्ता की खराब होती समस्या से जूझ रहा है जिसमें पी एम 2.5 की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के सालाना स्तर से भी 10 गुणा ज्यादा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि हमारे देश के तकरीब 1.36 अरब लोग पी एम 2.5 की उच्च सांद्रता की चपेट में हैं।
दावे कुछ भी किए जायें वायु प्रदूषण अब नासूर बन गया है। यह अब किसी खास मौसम की नहीं, बल्कि साल भर रहने वाली स्थायी समस्या बन चुकी है। यह तो अब लोगों की उम्र पर भी बुरा असर डाल रहा है। इससे जहां देश भर में रहने वाले लोगों की उम्र में 5.3 वर्ष की कमी आई है, वहीं राजधानी दिल्ली के लोगों की उम्र में 11.9 वर्ष की औसतन कमी आई है। शिकागो यूनीवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार पूरे भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरी उतरती हो। यह भी कि हृदय संबंधी बीमारियों से औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 4.05 वर्ष कम हो जाती है। जबकि बाल और मातृ कुपोषण से जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष कम हो जाती है। देश के सबसे प्रदूषित उत्तरी क्षेत्र में 52.2 करोड़ यानी 38.9 फीसदी आबादी वास करती है। यदि प्रदूषण का वर्तमान स्तर बरकरार रहता है तो इस आबादी की जीवन प्रत्याशा में ड्ब्ल्यू एच ओ के दिशा निर्देश के सापेक्ष औसतन आठ वर्ष व राष्ट्रीय मानक के सापेक्ष 4.5 वर्ष की कमी का खतरा है। भारत में 67.4 फीसदी आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जो भारत के खुद के बनाये मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्रदूषण को झेल रही है। कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी के शोध- अध्ययन से इसका खुलासा हुआ है कि यदि आप वायु प्रदूषण के बीच दो घंटे से अधिक समय भी रह लेते हैं तो इससे मस्तिष्क की फंक्शनल कनेक्टिविटी कम हो जाती है। अब तो यह साफ हो गया है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण का मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह जंगल की आग से निकलने वाले धुंए का भी स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खुले में हो रहे निर्माण से उड़ने वाली और सड़कों की धूल के चलते लोगों की जिंदगी धुंधली हो रही है। धूल में छोटे और बडे़ दोनों तरह के प्रदूषक मौजूद होते हैं। बडे़ आकार के प्रदूषक जैसे पी एम 10 और छोटे आकार के पी एम 2.5 होते हैं। पी एम 10 की वजह से ऊपरी श्वसन तंत्र, आंख और नाक में जलन और छोटे आकार के पी एम 2.5 के कण सांस के जरिये अस्थमा, गले का संक्रमण, सांस लेने में सी टी की आवाज आना, खांसी, त्वचा सम्बंधी बीमारी और ब्रोंकाइटिस के कारण होते हैं। ये इतने छोटे आकार के होते हैं कि खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाते हैं। इससे दिल की बीमारी और श्वसन तंत्र में अवरोध से अचानक होने वाली मौतों का खतरा बढ़ जाता है।
एम्स के फारेंसिक विभाग के अध्यक्ष डा. सुधीर गुप्ता के मुताबिक 22 फीसदी मौतों की मुख्य वजह श्वसन तंत्र में अवरोध है। सबसे जरूरी तो यह है कि लोगों को भी इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए कि वह किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं और वाहनों के धुंए जैसे नुकसानदायक वायु प्रदूषकों को कम करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं या नहीं। इस बाबत जागरूकता बेहद जरूरी है। साथ ही लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह मोटर साईकिल से या पैदल जाते समय कम व्यस्त सड़क पर ही चलें। यह सावधानी हमें काफी हद तक राहत दिलाने में मददगार हो सकती है। इस दिशा में चीन का उदाहरण प्रशंसनीय है। लेकिन चीन का अनुसरण कर पाना आसान नहीं है। इसमें वित्तीय संसाधनों की कमी और राजनीतिक दलों के आपसी टकराव तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी प्रमुख बाधा है जिसके चलते चीन का अनुसरण कर पाना असंभव है। हमारे यहां अक्सर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए किये जाने वाले ग्रेप जैसे उपाय केवल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम कर सकते हैं। जरूरत है प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारणों पर अंकुश लगाया जाये। निष्कर्ष यह कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अब सबसे बडा़ पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। फिर दिनोंदिन न्यूरोकाग्निटिव विकृतियां बढ़ने की घटनाओं को देखते हुए नीति निर्माताओं द्वारा इस मामले पर व्यापक स्तर पर विचार करना बेहद जरूरी है तभी कुछ बदलाव की उम्मीद संभव है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)