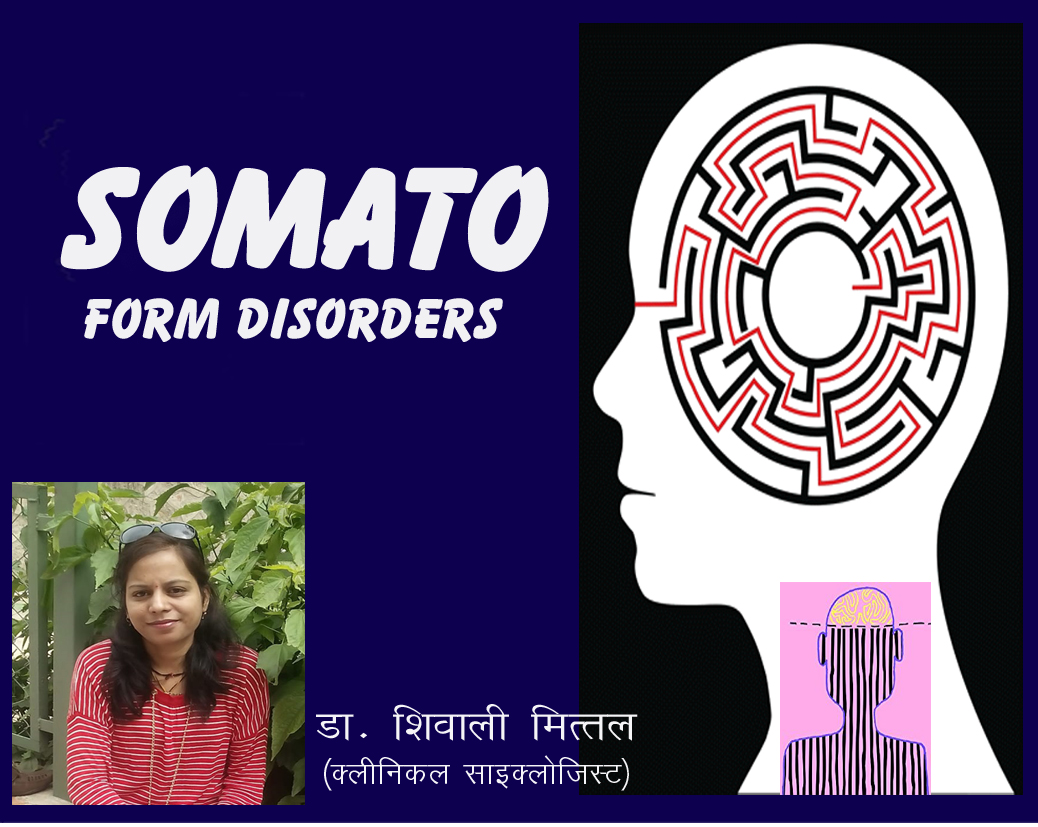लेखक : प्रोफेसर (डॉ.) सोहन राज तातेड़
पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान
www.daylife.page
धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत भावों की शुद्धता, मन की निर्मलता और सात्विक विचार का अधिक महत्व है। धर्म मूलतः किसी वस्तु का सहज गुण है। जैसे पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता और पृथ्वी का धर्म गंध है। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ है उन सबका स्वाभाविक धर्म होता है। जब पदार्थों में विकृति उत्पन्न की जाती है तो उनके गुण धर्म भी बदल जाते है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। यह अपने स्वरूप में चैतन्य युक्त है। शेष जितने भी पदार्थ है वे भौतिक तत्व है। उन पदार्थों में परिवर्तन, परिवर्धन होता रहता है। आत्मा और जड़ का जब संयोग होता है तो जड़ पदार्थ भी आत्मवत प्रतीत होने लगता है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। शरीर से जब आत्मा का संयोग होता है तो जड़ शरीर भी आत्मवत् प्रतीत होने लगता है। शरीर से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य किये जाते है।
मूलतः आत्मा के शुद्धि और अशुद्धि का कोई प्रश्न नहीं है। शरीर में शुद्धता और अशुद्धता देखी जाती है। यदि मानव अच्छा कर्म करता है तो पुण्यलोक की प्राप्ति होती है और यदि बुरा कार्य करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसीको ध्यान में रखकर यह बात कही गयी है कि धर्म आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न वाणी से कहा जा सकता है, न तो अन्य इन्द्रियों से उसे जाना जा सकता है, न तपस्या और कर्म से ही उसे जाना जा सकता है। जिसके द्वारा सारी ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने विषय का ज्ञान कराती हैं उसे किस साधन से जाना जाय। इसलिये कहा गया है कि ‘ज्ञानप्रसादेन तं पश्यते’ अर्थात् ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। जप, तप निखिलकर्मानुष्ठान ये सारे साधन आत्मविषयक आचार में परिगणित हैं, किन्तु ये केवल चित्त शुद्धि तक ही सीमित हैं। शुद्ध चित्त में ज्ञान का प्राकट्य उसी प्रकार होता है जैसे स्वच्छ कांच में प्रतिबिम्बोपलब्धि होती है। पुरुष या आत्मा को चेतन तत्त्व तथा प्रकृति को अचेतन या जड़तत्त्व कहा गया है।
पुरुष के स्वरूप को बतलाते हुये यहां कहा गया है कि पुरुष नित्य, साक्षी, केवल, निस्त्रैगुण्य, माध्यस्थ उदासीन, द्रष्टा और अकर्त्ता है। पुरुष चेतन है। चेतन ही विषयों का ज्ञाता तथा द्रष्टा होता है। इसे अचेतन नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मा ही वह द्रव्य है जिसमें बुद्धि, सुख-दुःख, राग-द्वेष, इच्छा प्रयत्न आदि गुण रहते हैं। ये गुण शरीर के नहीं आत्मा के ही हो सकते हैं। आत्मा देह, इन्द्रिय आदि से भिन्न है, नित्य और व्यापक है। मन से उसका प्रत्यक्ष होता है तथा मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं इत्यादि से आत्मा का अस्तित्त्व प्रकट होता है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। पत्ते पर स्थित ओस बिन्दु की तरह हवा के झकोरे खाकर नाशवान है। इस छोटे से आयु खंड में जिसने जितना धर्म कर्म कर लिया उसका जीवन उतना ही सार्थक है और जिसने व्यर्थ में ही जीवन को गवा दिया वह अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया।
जीवनकाल में धर्म ही मनुष्य को त्राण दे सकता है। धर्म की व्याख्या करने के लिए इसके लौकिक और पारलौकिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। लौकिक धर्म वह धर्म है जिसे हम इस लोक में करते है और उसका फल भोगते है। पारलौकिक धर्म इस लोक से परे है और वहीं मानव जीवन की सच्ची कमाई है। इसी धर्म को प्राप्त करने के लिए मानव को प्रयास करना चाहिए। इस तथ्य की सत्यता को हृदयंगम कर भारतीय ऋषियों ने अपने वेद ज्ञान के संस्मरणों, निष्कर्षों को स्मृति शास्त्र के रूप में मानव समाज के हितार्थ प्रगट किया। जिससे वे भोगवाद की आसुरीधारा में न बहकर आत्मकल्याण का सर्वप्रथम ध्यान रखें और अर्थ तथा काम के साथ ही धर्म और मोक्ष के साधन के लिये भी प्रयत्नशील रहें। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तभी सम्भव है, जब वह अपना आचरण शुद्ध रखे और संयम नियम का पालन करता रहे।
मलिनता और अपवित्रता चाहे बाह्य हो अथवा चाहे आन्तरिक, मनुष्य के उच्चभावों को नष्ट करके उसे पाप कर्मों की तरफ प्रेरित करती हैं। इसलिये मानव को सुसंस्कारित बनाने के उद्देश्य से अनेक नियम बनाये गये है, जिससे वे अनुशासन, मर्यादा, नैतिकता आदि की शिक्षा प्राप्त करके वास्तविक मनुष्यता का विकास कर सकें। जन्म के समय मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में विशेष अन्तर नहीं होता, वरन् यदि देखा जाय तो मनुष्य का नवजात शिशु अन्य पशुओं के बच्चे की अपेक्षा अधिक असमर्थ और असहाय स्थिति में होता है। कुछ बड़ा होने पर भी वह स्वयं कोई नयी बात कर सकने में असमर्थ होता है। परिवार और समाज तथा अपने चतुर्दिक वातावरण से वह बहुत कुछ सीखता है।
इसलिये जैसे संस्कार उसमें डाले जायेंगे वैसा ही आचरण वह समाज में करेगा। जिस देश काल व समाज में आचारण की जो पवित्र परम्परायें चलती रहती हैं, वह सदाचार है। सदाचार एक ऐसा व्यापक सार्वभौम तत्त्व है जो देश काल की संकीर्ण सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता-जैसे सूर्य की रश्मियां सारे संसार के लिये उपयोगी होती हैं, उसी प्रकार सदाचार भी प्राणिमात्र के लिये उपयोगी होता है। अहिंसा, सत्यादि का पालन मानव को करना चाहिए। महाभारत में वेदव्यास ने भी यही कहा है कि सभी आगमों में आचार ही प्रधान है-‘सर्वागमानां आचारः प्रथमं परिकल्पते’। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। आचार धर्म का मेरुदण्ड है, जिसके बिना धर्म टिक नहीं सकता। आचार का पालन करने वाला मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसीलिए धर्म को आत्मशुद्धि का साधन माना गया है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)